1. कल्याणकारी व्यवस्था :-
राज्य अपने नागरिकों के लिए कल्याणकरी व्यवस्था करेगा | कल्याणकारी व्यवस्था से तात्पर्य लोगों के कल्याण से है , चाहे वह आम नागरिक हो अथवा श्रमिक । इसके अंतर्गत आवास , बिजली , पेयजल , मनोरंजन , शिक्षण - प्रशिक्षण , शिशुगृह इत्यादि शामिल हैं । कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कल्याण एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है ।
2. समाजवादी व्यवस्था :-
समाजवादी से तात्पर्य समाज में संपत्ति या आर्थिक एकसमान होती समानता स्थापित करने से है । अर्थात वंटवारा समाज के सभी लोगों के बीच चाहिए । इसी आधार पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को नियोजक के लाभ से वितरित किया जाता है ।जैसे : मजदूरी , वोनस , महंगाई भत्ते आदि में वृद्धि करना | उहाहरण : - बोनस अधिनियम 1965 पारित किया जा चुका है ।
3. मौलिक अधिकार ( अनुच्छेह 12 से 35 )
इसमें श्रम से संबंधित निम्न उपबंध किए गए हैं :-
A) समानता का अधिकार :-
विधि के समय समानता ( अनुच्छेद -14 ):-
भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता ही जाएगी । अर्थात वह भारत के किसी भी न्यायालय में अपील कर सकता है । भारतीय श्रमिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है । इसी आधार पर औद्योगिक विवाह अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय , अधिकरण एवं राष्ट्रीय अधिकरण का गठन किया जाता है|
भेद - भाव पर रोक ( अनुच्छेह . 15 ) :-
राज्य जाति , धर्म , मूलवंश लिंग , भाषा , आदि के आधार पर कोई भेद - भाव नहीं करेगा | इसी आधार पर उद्योगों में काम कसे वाले श्रमिकों के साथ किसी प्रकार का गेंद - भाव नहीं किया जाता है ।
अवसर की समानता ( अनुच्छेद-16) :-
राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान अवसर की व्यवस्था करेगा । उन स्थितियों को छोड़कर जहाँ पिछड़े वर्ग के , लिए आरक्षण हो । इसी आधार पर कारखानो में श्रमिकों के लिए समान अवसर की व्यवस्था की गई है ।
अस्पृश्यता का अंत ( अनुच्छेद -17 ):-
राज्य अस्पृश्यता का अंत करेगी। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों, भोजनालयों, मंदिर - मस्जिद में प्रवेश आदि में अस्पृश्यता के आधार पर रोउ नहीं रहेगा । यदि कोई व्यक्ति इस पर प्रतिबंध लगाता है तो दण्डित किया जाएगा । इसी आधार पर कारखानों में श्रमिक कहीं भी प्रवेश कर सकता है अथवा भोजन कर सकता है ।
बेगार पर रोक ( अनुच्छेद- 23 ):-
भारत के किसी भी नागरिक से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता है । इसके निवारण के लिए बंधुआ मजदा उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया है ।
बालश्रम पर प्रतिषेध :-
14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने अथवा रखतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता है । इसी आधार परबाल श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियम ) अधिनियम- 1986 पारित किया गया है ।
4. नीति निर्देशक तत्व ( अनुच्छेद 36 से 51 ):-
इसमें श्रम से संबंधित निम्न उपबंध वर्णित है :-
अनुच्छेद -38:-
राज्य अपने नागरिकों के लिए कल्याण की व्यवस्था करेगा ! अर्थात कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा । जैसे : आवास , बिजली , पेयजल, शिक्षण एवं प्रशिक्षण , केंटिन , शिशु गृह , इत्यादि जो श्रमिक पर भी लागू होता है ।
अनुच्छेद -39:-
राज्य अपने नागरिकों के लिए समाजवादी व्यवस्था स्थापित करेगा । अर्थात सम्पत्ति का वंटवारा एक समान किया जाएगा । इसी आधार पर नियोजन के लोगो से श्रमिकों में वितरित किया जाता है ।
समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किया जाएगा । ताकि सामाजिक न्याय की अवधारणा विकसित हो । इसी आधार पर समान काम के लिए समान वेतन संबंधी कानून बनाए गए है । उहाहरण :-समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 । नवम्बर 2016में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी पूर्णत : व्याख्या की है ।–
राज्य अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था करेगा । विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों के स्वस्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था डी जाएगी । उहाहरण कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत स्वस्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ।
अनुच्छेद 41:-
राज्य विभिन्न आकस्मिकताओं की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगी । इसी आधार पर असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 गए हैं । उपाहान संदाय अधिनियम 1972 इत्यादि पारित किएगए हैं।
अनुच्छेद 42:-
राज्य महिलाओं को प्रसुति संरक्षण की व्यवस्था करेगी | इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 पारित किया गया है ।
अनुच्छेह 43A :-
राज्य कारखानों में प्रबंधन में श्रमिकों को सहभागिता स्थापित करने का प्रयास करेगा | इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा उद्योगों में कई संस्थाए स्थापित की जाती है । जैसे कार्य समिति , संयुक्त प्रबंधन परिषद , कर्मशाला परिषद , झाई परिषद् , संयंत्र तल , सौप ( shop ) तल , इत्यादि ।
अनुच्छेद 47 :-
राज्य अपने नागरिकों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था करेगा । इसी आधार पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था की गई है ।
5. विधायी शक्तियों का विभाजन : -
अनुच्छेद 246 में विधायी शक्तियों से संबंधित प्रावधान वर्णित है । इसमें तीन सूची ही गई है : - संघ सूची , राज्य सूची समवर्ती सूची |
संघ सूची :-
संघ सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है । इसके अन्तर्गत निम्न विषय शामिल हैं . जैसे रेलवे सेवा , डाक् सेवा , बन्दरगाह ILO में प्रतिनिधि भेजना , श्रम सम्मेलनों में भाग लेना इत्यादि ।
राज्य सूची:-
राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है । इसके अंतर्गत राज्य पेंशन , बेरोजगारी भत्ता , आदि शामिल हैं ।
समवर्ती सूची:-
समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को है । लेकिन विवाद की स्थिति में केन्द्र द्वारा बनाई गई कानून प्रभावी होगा । इसके अंतर्गत कई विषय शामिल किया गया है जैसे औद्योगिक संबंध , औद्योगिक बिवाद , विवाद सुलझाने के तरीके , सामुहिक सौदेबाजी , प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता , रोजगार सृजन इत्यादि ।
अनुच्छेद 256:-
केंद्र सरकार राज्य सरकारो को निर्देश देगी की वह अपने राज्य क्षेत्र में कानून पारित करें । इसी आधार पर बिहार सरकार द्वारा बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 पारित किया गया है ।
अनुच्छेद 257:-
केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश होगी कि केन्द्र द्वारा बनाई गई कानून को अपने राज्यों में लागू करें । उदाहरण : - कार्य स्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम ( 2013 ), असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 , कारखाना अधिनियम 1948 इत्यादि केन्द्रीय कानून है जिसे राज्यों में राज्य सरकार लागू करती है ।
इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रमिकों के हितों एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं । परिणामस्वरूप श्रम की दशाओ में बेहतर सुधार लाने का प्रयास किया गया है । लेकिन बहुत से ऐसे उद्योग है जहाँ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है । अत : इसमें कई कमियाँ बताई जा रही है :
- संवैधानिक प्रावधानों का सरकार द्वारा सही तरीके से क्रियान्वयन नही किया जा रहा है । कानून तो बनाई जाती है । लेकिन प्रशासनिक प्रतिवद्धता . सरकार एवं श्रमिकों के बीच समन्वय का अभाव में ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाती है । अत : इसमें सुधार करने की आवश्यकता है
-पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हावी है । नई आर्थिक नीति लागू होने के पश्चात बहुत से कानून नियोजन के पक्ष में बनाए गए हैं । आज भी प्रबन्ध में श्रमिकों की सह मागिता संबंधी अलग से विधिक प्रावधान नहीं है । अत : समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास होना चाहि ।
-किसी भी कानून के क्रियान्चयन के लिए लोग , श्रमिकों को शिक्षित होना अनिवार्य है । लेकिन भारत के अधिकांश श्रमिक अशिक्षित है । नियोजक उनकी अशिक्षा का लाभ उठाकर शोषण करता है । अत : इन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है ।
- संवैधानिक भावना को देखते हुए जितने भी श्रम कानून पारित किए गए हैं , उसमे दण्ड की व्यवस्था बहुत ही कम है | नियोजक बार - बार अधिनियम का उल्लंघन करता है । अत : कड़ी से कड़ी दण्ड की व्यवस्था होना चाहिए।
इस प्रकार उपरोक्त कमियों को दूर किया जाए तथा संविधान की मूल भावना को ध्यान में श्रम कारों का कियान्वयन किया जाए तो श्रमिकों की दशाओं में बेहतर सुधार होगा । औद्योगिक विकास होगा । देश की आर्थिक विकास एवं प्रगति होगी।
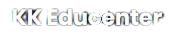
Post a Comment
We welcome relevant and respectful comments. Off-topic or spam comments may be removed.